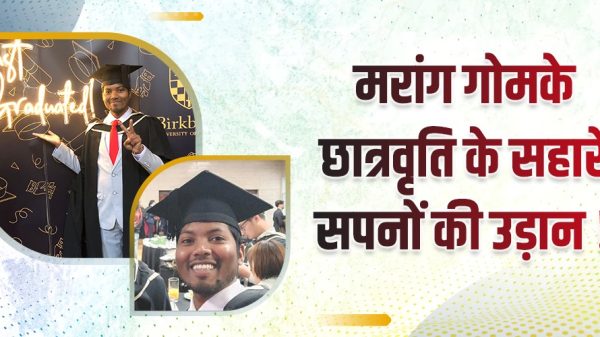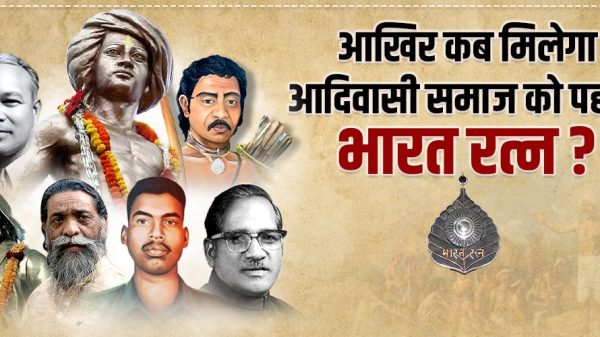अनेक मंच और विश्व पटल पर जब भी किसी आदिवासी समाज की बात होती है तो अमूमन एक जंगल में निवास करने वाला और विचित्र वेशभूषा के साथ अपने त्वचा को रंगा एक छवि प्रस्तुत की जाती है। 21 वीं शताब्दी में भी विशाल जनमानस आदिवासी को जंगली ही मानते हैं। परिवर्तन एक अटूट सत्य है और जब सभी समाजों में परिवर्तन हुआ है, तो आदिवासी समाज में भी परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए? लोग अचंभित होते हैं जब एक आदिवासी ‘वृहद् समाज’ का अंग बनता है।
आदिवासी समाज में भी परिवर्तन हुआ है, किंतु वह धीमी गति से हुआ है। इसका एक ठोस वैज्ञानिक कारण है। पुरातत्व मानवशास्त्र में एक विख्यात सिद्धांत है। पुरातन काल में मनुष्य की आवश्यकताएँ सीधे प्रकृति से पूरी होती थी। मनुष्य आवश्यकता अनुरूप प्रकृति से संसाधन प्राप्त करता था। धीरे धीरे यह आवश्यकता पूंजीवाद में बदला और फिर प्रकृति का दोहन अनियंत्रित हो गया। औद्योगिक क्रांति के बाद ‘लोभ’ ने पूंजीवाद को अपने चरम पर पहुँचा दिया। आवश्यकता अनंत होतीं चली गयीं और संसाधन सीमित। दोहन की परिधि स्थानीय से बढ़कर अंतरराष्ट्रीय हो गयी।
वहीं, आदिवासी समाज के जीवन दर्शन में प्रकृति की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके जीवनशैली में प्रकृति और पर्यावरण उनके स्वयं के जीवन के अभिन्न अंग थे। इसलिए प्रकृति का दोहन उनके समाजिक सांस्कृतिक नियम क़ानून के द्वारा नियंत्रित ढंग से होती थी। सामूहिक ‘संपत्ति’ की अवधारणा ने ‘लोभ’ को दूर रखा। स्वयं में वो एक आत्मनिर्भर समाज थे। आवश्यकता सीमित थी तो दोहन भी सीमित रहीं। जब ये सभी तथ्य नियंत्रित रहें, तो समाज को वृहद् परिवर्तन की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसलिए, इस गूढ़ तथ्य को समझना होगा कि आदिवासी समाज में परिवर्तन ‘सतत जीवनशैली’ की अवधारणा पर आधारित है। आदिवासी ‘विकास विरोधी’ नहीं है और ना ही ‘कम बौधिक’ क्षमता वाला है। उनके समृद्ध देशज ज्ञान ने हमेशा से विश्व को आकर्षित किया है और अब तो संयुक्त राष्ट्र से लेकर अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठन इस ज्ञान को पृथ्वी के संरक्षण में लगाना चाहते हैं। सर्वमत से आज विश्व समुदाय ‘जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए आदिवासी जीवनशैली की ओर आस से देख रहा है।
किंतु अब परिस्थियाँ तेज़ी से बदल रहीं हैं। जब तक आपका गाँव आपका देश था, उपरोक्त बातें अर्थपूर्ण थीं। पर अब हम गाँव से निकल चुके हैं, या ‘अन्य’ की पहुँच आपके गाँव तक हो गयी है। हम बहुजातीय समाज के अविभाज्य अंग बन गए हैं। अब आदिवासी जीवन पूर्णतः पृथक और आत्मनिर्भर नहीं रह गया है। आधुनिक जीवन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार अनिवार्य हो गए हैं। ऐसे में आदिवासियत कहीं बहुत पीछे छूट गयी है।जब तक शिक्षा नहीं होगी, चुनौतियाँ कभी कम नहीं होंगी। और आदिवासियत बचेगी नहीं तो आपके अस्तित्व पर ही प्रश्न उठ खड़ा होगा।
आज अनेक समाज आपके रीति रिवाजों को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उन्हें आदिवासियत प्राप्त हो सके। अनेक धर्म और वृहद् समाज हैं जो आपके प्राकृतिक धर्म को स्वयं के समकक्ष दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप उस भीड़ में समाहित हो सकें। ऐसे समय में समाज को सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी और से नहीं अपितु स्वयं का आँकलन अति आवश्यक होता जा रहा है।
आदिवासी समाज स्पष्ट रूप से दो वर्ग में विभाजित है। एक शहरी और दूसरा ग्रामीण। ग्रामीण क्षेत्र प्रमुखता से आदिवासियत को आत्मसाथ किया हुआ है किंतु आधुनिकता में पीछे है। वहीं दूसरी ओर शहरी आदिवासी आधुनिकता में डूबे हुए हैं और आदिवासियत नगण्य होती जा रही है। आधुनिकता का अर्थ इस चर्चा में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार से है। वर्तमान परिवेश में आधुनिकता और आदिवासियत में संतुलन अनिवार्य है। बिना आदिवासियत के अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य बने रहना निकट भविष्य में चिंता का विषय हो सकता है। समझना होगा कि यह अस्थायी अधिकार है।
आप पौधा लगाते हैं, पेड़ नहीं। यदि यह चेतना आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित नहीं होगी तो निकट भविष्य में यह सारा प्रयास औंधे मुँह गिरेगा। आदिवासी समाज में जो जागरूकता और चेतना हाल के दिनों में देखने मिली है वह संतोषजनक है। किंतु यदि आने वाली पीढ़ी को तमाम समाजिक एवं सांस्कृतिक प्रयास से दूर रखेंगे तो यह एक छलावा मात्र होगा। माय माटी में ‘धुमकुड़िया’ आलेख के आने के बाद डॉ नारायण उराँव ‘सैंदा’ ने सुखद अनुभव साझा किया। उन्होंने अपने दोनो पुत्र को वर्षों पहले पारंपरिक रूप से अपने गाँव में ‘धुमकुड़िया’ में प्रवेश कराया था। इस प्रकार का प्रयास हमें अपने आने वाली पीढ़ी के साथ करना ही होगा। करम, सरहूल, रोपा इत्यादि से संबंधित गीत सीखाना होगा, हल बैल, खेत खलिहान, से जोड़ना होगा। पारंपरिक वाद्य यंत्र से जोड़ना होगा। अपनी आदिवासियत पर गर्व करने सीखाना होगा। सप्ताह में एक बार सरनास्थल ले जाकर पुरखों को और प्रकृति से विनती-याचना सीखाना होगा। तेज़ी से विलुप्त होती आदिवासी नैतिकता और मौलिकता को पुनर्जीवित करना होगा। यह सम्भव है क्योंकि मैंने अपने दोनो पुत्रों को यह सिखाया है। इसलिए मुझे विश्वास है कि अन्य आदिवासी अभिभावक भी इस प्रकार का प्रयास करेंगे और वो निश्चित सफल होंगे। और जब आपका ‘पौधा’ हमारी गुम होती आदिवासियत को पुनः जिएगा, वह अनुभूति अलौकिक होगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के आदिवासी समाज के समग्र विकास के लिए उनका सहयोग करना ही होगा। इस खाई को अनेक माध्यम से पाटने का प्रयास होना चाहिए।
प्रभात खबर के माय माटी में आलेख आने पर विभिन्न प्रतिक्रिया महानुभावों से प्राप्त होता है। कुछ एक ऐसे भी होते हैं तो मेरी लेखनी को ‘नकारात्मक’ मानते हैं। उनका कहना है कि आदिवासी जीवन शैली काफ़ी समृद्ध है और मेरे लेख मात्र ‘उदासीन पक्ष’ को दर्शाते हैं। उनकी टिप्पणी का मैं आदर करता हूँ किंतु स्पष्टीकरण के साथ। नकारात्मक होना और आत्म आलोचना करने में अंतर है। मेरा बड़ा तार्किक प्रश्न है। यदि हम आज भी त्रुटियों को नजरंदाज करेंगे तो समाज की बेहतरी कैसे होगी। हमारा आदिवासी समाज समृद्ध है, पर क्या आप हमारे समाज के वर्तमान परिस्थितियों से संतुष्ट हैं?
आज विश्व, आदिवासी जीवन शैली को बड़े ही सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहा है, पर क्या हम स्वयं इस तथ्य को सराहते हैं? शायद नहीं। मेरी लेखनी का उद्देश्य ही यही है। विख्यात फ़िल्म निर्माता मेघनाथ दा निरंतर प्रोत्साहित करते हैं, और उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज में आदिवासियत बचाए रखने के लिए ‘नवजागृति’ या ‘रेनेसां’ आवश्यक है। ऐसे में अमृत्सव में भी आदिवासी समाज के अनेक प्रभुद्ध जानो को विष तो पीना ही पड़ेगा।

लेखक परिचय:
डॉ. अभय सागर मिंज एक अंतर्राष्ट्रीय-स्तर के जाने-माने शिक्षाविद हैं, जो संप्रति डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (रांची) के मानवशास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापक के तौर पर कार्यरत हैं। आधुनिकता की चुनौती से जुझते आदिवासी समाज को आदिवासियत और आधुनिकता में संतुलन बनाने की वकालत करता उनका यह बहुचर्चित आलेख 7 अक्टूबर 2022 को प्रभात खबर में प्रकाशित हो चुका है।