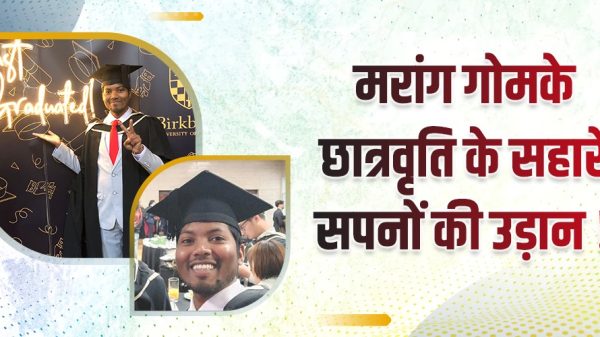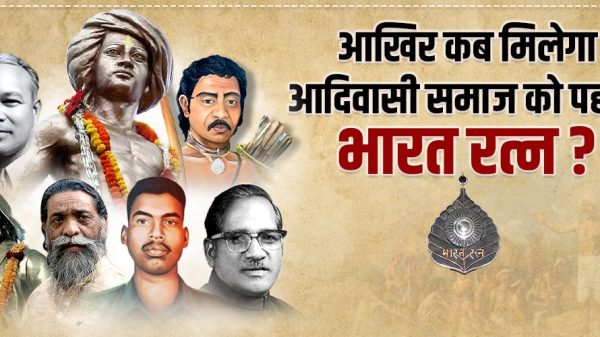प्राचीन काल में जब प्रकृति अपने कुदरती अवस्था में थी तब परिवारों के एक झुंड ने कुदरती प्रकृति में परिवर्तन कर के जंगल की सफ़ाई की और उसे खेती योग्य भूमि में परिवर्तित किया। स्थायी जीवन की शुरुआत के लिए यह प्रथम चरण था। मनुष्य नव पाषाण काल में खेती की शुरुआत आज से दस हज़ार वर्ष पूर्व शुरू करता है। जैसे ही मनुष्य को बीज का महत्व पता चला और झुंड की जनसंख्या बढ़ती चली गई वह स्थिर जीवन के लिए बाध्य होता है। जंगल की सफ़ाई किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार के बस की बात नहीं थी। अनेक परिवार मिल कर इस कार्य को करते हैं। और इस तरह एक आदिवासी गाँव स्थापित हो जाता है। अथक परिश्रम से खेत का निर्माण होता है और चूँकि यह एक सामूहिक प्रयास था इसलिए इन भूमि पर सबका बराबर का अधिकार स्थापित हो जाता है। सामूहिकता पर आधारित एक आदिवासी गाँव का निर्माण होता है। यही मज़बूत आधार इस समाज की विशिष्टता भी बनती है। कहने का अर्थ है कि यहाँ किसी की निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी। जो आपका है वो मेरा भी है। जितना अधिकार प्रकृति संसाधनों पर मेरा है उतना ही आपका भी। इस अवधारणा पर जनजातीय समाज का पूरा जीवन दर्शन केंद्रित है।
इस सामूहिक स्वामित्व और निजी संपत्ति की अवधारणा का अभाव ने आदिवासी समाज को ‘बेहिसाब, अंतहीन लालच’ से हमेशा दूर रखा। जितना आवश्यक था उतना उत्पादन होता था। और यह जीवित रहने के लिए पर्याप्त था। मुद्रा का अस्तित्व, आदिवासी समाज के अंदर पिछले सदी तक नहीं था। अचल संपत्ति में भूमि और चल संपत्ति में पशु, आभूषण, पत्थर के औज़ार इत्यादि। आदिवासियों में आभूषण का सामाजिक मूल्य उनके आर्थिक मूल्य से अधिक था। आभूषण का आर्थिक मूल्य विशेष महत्व नहीं रखता था क्योंकि आभूषण व्यक्तिगत शृंगार तक सीमित था। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित हो कर सामाजिक संबंध को प्रगाढ़ बनाता था। आभूषणों का कोई विशेष आर्थिक मूल्य इसलिए भी नहीं होता था क्योंकि प्राचीन आदिवासी समाज में क्रय विक्रय की परंपरा ही नहीं थी। उन्हें बेच कर वे क्या ही ख़रीदते?
सामूहिक स्वामित्व ने कभी भी चल और अचल संपत्ति के व्यक्तिगत संचय की ना तो प्रथा थी ना ही आवश्यकता। यह सामूहिकता आदिवासी समाज की नींव थी। चाहे वह अनाज हो, शिकार हो, या कंद मूल संकलन, ये सभी बराबर मात्रा में समूह के परिवारों में वितरित होते थे। यह आज भी है। अपने बाल्यावस्था में जब मैं गाँव में सामूहिक रूप से पहली बार नदी में मछली मारने गया था तो सामूहिक प्रयास ने बहुत प्रभावित किया था। सभों को अपना कार्य विभाजित किया गया था। यह सामूहिक दायित्व ने कार्य को रोचक और सरल बना दिया था। तत्पश्चात् दो आश्चर्य करने वाली प्रक्रियाएँ देखने को मिली। पहल तो पकड़े गये मछलियों में से छोटे आकार के मछलियों को धार्मिक क्रिया के बाद वापस नदी में छोड़ दिया गया। सतत् विकास और प्रकृति के प्रति आभार के उदाहरण ने मन छू लिया। ये छोटी मछलियाँ अब बीज का काम करतीं। दूसरा यह हुआ कि पकड़े गये मछलियों का विभाजन गाँव में प्रत्येक परिवार के आधार पर किया जाने लगा। वितरण प्रणाली से मैं असहज और व्याकुल हो उठा। गाँव के बुजुर्ग, विभाजन में उन परिवारों को भी हिस्सा दे रहे थे जो उस दिन किसी कारण वश मछली पकड़ने साथ नहीं आये थे। मैंने अपने पिता से पूछा कि ऐसा क्यों? तब गाँव के ही एक बुजुर्ग ने समझाया कि “बाबू यह जल, जंगल, ज़मीन, नदी, पहाड़ हम सभों का बराबर है। वो नहीं भी आये पर इनपर उनका भी अधिकार है। हाँ उनको थोड़ा कम हिस्सा मिलेगा, पर मिलेगा जरूर”। आदिवासियत पर गर्व हुआ।
इस उदाहरण की चर्चा यहाँ इसलिए सार्थक है क्योंकि सामूहिक स्वामित्व स्पष्ट हो सके। इस प्रकार के सामाजिक संरचना में निजी संपत्ति का संचय अर्थहीन था। यह आदिवासी समाज की एक बहुत ही गूढ़ विशिष्ठता है। इस सामूहिक स्वामित्व ने धन और संसाधन के व्यक्तिगत संचय को रोके रखा। और जब भी पर्यावरण और वातावरण से संसाधन का दोहन हुआ तो वह हमेशा आवश्यकता अनुसार और नियंत्रित हुआ। जितना आवश्यक था उतना संसाधन, पर्यावरण से प्राप्त किया गया। जब लालच नहीं था, सात पीढ़ियों के संचय की अवधारणा नहीं थी, तो आदिवासी समाज अपने आप में संतुष्ट, समर्थ और संतुलित था। सामाजिक विज्ञान में यह प्रमाणित तथ्य है कि यदि समाज आंतरिक रूप से तृप्त और संतुलित है तो वैसे समाज में परिवर्तन या बदलाव की गति बहुत धीमी होती है। यहाँ वृहद् परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं थी। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक होता है कि यदि वर्तमान विद्यमान सामाजिक संरचना अपने दायित्वों और आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है तभी परिवर्तन होता है।
आदिवासी युवाओं को अपने इस समृद्ध जीवन शैली पर गर्व करना चाहिए। यह कहीं से भी संकोचित होने वाली बात नहीं है कि आपके ‘विकास’ को एक अलग हेय की दृष्टिकोण से दुनिया देखती है। पृथ्वी में संसाधन सीमित हैं, और जिस गति से इन संसाधनों का दोहन हो रहा है, पृथ्वी एक दो सदी तक पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन के विद्वान मानते हैं कि हम उस चरण में अब प्रवेश कर चुके हैं जहाँ हम आज उन सभी प्रकार के जलवायु परिवर्तन की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें तब भी पृथ्वी को अर्ध मूर्छित अवस्था से वापस नहीं ला सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन के इकाई ने इसे ही ‘पॉइंट ऑफ़ नो रिटर्न’ कहा है।
वहीं दूसरी ओर, एक पूँजीवादी समाज ने आर्थिक उन्नति को ही विकास का पर्यायवाची मान लिया था। जहाँ विश्व के अन्य समाज में निजी संपत्ति की अवधारणा थी, वहाँ व्यक्तिगत धन संचय निरंतर उग्र होती चली गई। पहले सामन्तवाद के रूप में फिर पूंजीवाद के रूप में। औद्योगिक क्रांति के बाद यह और प्रखर होता चला गया। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह आवश्यकता लोभ में परिवर्तित हो गई। यूरोप के छोटे छोटे देश औद्योगिक क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। व्यापार अब अंतर देशीय हो गया। मांग और आपूर्ति का सानिध्य लाभ से हो गया। और अंततः लाभ का ‘लोभ’ से हो गया। अब लाभ और ‘लोभ’ अंतहीन हो गई और इस लाभ और लोभ को पूरा करने के लिए समाज में तेज़ी से अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। पर्यावरण का हनन और दोहन अपने चरम पर आ गया। वर्तमान में स्तिथि और वीभत्स होती जा रही है और हम में से कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन ने व्यक्तिगत संबंधों को कमज़ोर कर दिया है।
उपरोक्त विचार दर्शाते हैं कि आदिवासी समाज में परिवर्तन नियंत्रित रहा क्योंकि उनका जीवनशैली पर्यावरण का उपभोग संयम और सतत् प्रक्रिया के साथ करता रहा और इसलिए उनमें बदलाव बहुत धीमी गति से हुई । यह विडंबना ही है कि आदिवासियों के नियंत्रित पर्यावरण उपयोग को असभ्य और आदिम माना गया।उनके मौलिक तत्वों को बहुत देर से अब आत्म साथ करने का प्रयास हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के समागम 107 और 169 के साथ साथ 2015 के पैरिस समझौता इस बात पर ज़ोर देते हैं कि यदि पृथ्वी को बचाना है तो आदिवासी ज्ञान परंपरा और आदिवासियों को, जलवायु परिवर्तन के संघर्ष में साथ लेकर चलना होगा। वहीं वर्तमान आधुनिक समाज में परिवर्तन की गति अब अनियंत्रित हो गई है। हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, यह मंथन करने का शायद हम में से किसी के पास समय भी नहीं है।
इस परिचर्चा में विकास की परिभाषा और संबंधित दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण कारक है। एक आधुनिक समाज के लिए किसी व्यक्ति के समग्र आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और स्वास्थ्य उन्नति, विकास के प्रतीकात्मक तत्व हैं। किंतु इस विकास की परिभाषा में यह सुस्पष्ट है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य जैसे घटक भी मूल रूप से आर्थिक सबलता पर पूरी तरह से निर्भर और केंद्रित है। वहीं आदिवासी समाज में विकास का मानदंड व्यक्ति विशेष ना होकर सामूहिक होता है।
तत्कालीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉ बी डी शर्मा कहते हैं कि विकास की परिभाषा को लेकर हमें पुनः विचार करना चाहिए और अपने दृष्टिकोण का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए। विकास का मानदंड जो हम अपने आधुनिक समाज में लागू करते हैं, वो आवश्यक नहीं कि आदिवासी समाज के लिए भी उतना ही प्रभावी हो। विकास की प्रक्रिया किसी भी समाज के लिए स्वीकार्य हो, वह बाहर से थोपा ना गया हो और यह एक समावेशी विकास प्रक्रिया को आत्म साथ करने का प्रयास हो। नहीं तो हम भी अंग्रेजों के ‘वाइट मैंस बर्डन’ के सिद्धांत के अनुरूप आदिवासी समाज को समझाने और विकसित करने का निरर्थक निरंतर प्रयास करते रहेंगे। जबकि आज ठीक विपरीत, पूरा विश्व आदिवासी समाज के जीवन सार से सीखने का प्रयास कर रहा है।
लेखक परिचय:
डॉ. अभय सागर मिंज एक अंतर्राष्ट्रीय-स्तर के जाने-माने शिक्षाविद हैं, जो संप्रति डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (रांची) के मानवशास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापक के तौर पर कार्यरत हैं। आदिवासी समाज में विकास तथा प्राकृतिक संतुलन के जीवन दर्शन की बात करता उनका यह बहुचर्चित आलेख 28 अप्रैल 2023 को प्रभात खबर में प्रकाशित हो चुका है।